CBSE Class 10 Hindi A Unseen Passages अपठित गद्यांश

अपठित गद्यांश CBSE Class 10 Hindi A Unseen Passages अपठित गद्यांश
NCERT Solutions for Class 10 Hindi Kshitij, Kritika, Sparsh, Sanchayan are the part of NCERT Solutions for Class 10. Here we have given CBSE Class 10 Hindi NCERT Solutions of क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन.
Please find Free NCERT Solutions for Class 10 Hindi Sanchayan, Sparsh, Kshitiz, Kritika in this page. We have compiled detailed Chapter wise Class 10 Hindi NCERT Solutions for your reference.
CBSE Class 10 Hindi A Unseen Passages अपठित गद्यांश . is part of NCERT Solutions for Class 10 Hindi. Here we have given CBSE Class 10 Hindi A Unseen Passages अपठित गद्यांश .
CBSE Class 10 Hindi A Unseen Passages अपठित गद्यांश Textbook Questions and Answers
अपठित बोध
अपठित बोध ‘अपठित’ शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ‘unseen’ का समानार्थी है। इस शब्द की रचना ‘पाठ’ मूल शब्द में ‘अ’ उपसर्ग और ‘इत’ प्रत्यय जोड़कर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है-‘बिना पढ़ा हुआ।’ अर्थात गद्य या काव्य का ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो। परीक्षा में अपठित गद्यांश और काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य छात्रों की समझ अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक योग्यता का परख करना होता है।
अपठित गद्यांश
अपठित गद्यांश अपठित गद्यांश प्रश्नपत्र का वह अंश होता है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों से नहीं पूछा जाता है। यह अंश साहित्यिक पुस्तकों पत्र-पत्रिकाओं या समाचार-पत्रों से लिया जाता है। ऐसा गद्यांश भले ही निर्धारित पुस्तकों से हटकर लिया जाता है परंतु, उसका स्तर, विषय वस्तु और भाषा-शैली पाठ्यपुस्तकों जैसी ही होती है।
प्रायः छात्रों को अपठित अंश कठिन लगता है और वे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसका कारण अभ्यास की कमी है। अपठित गद्यांश को बार-बार हल करने से –
- भाषा-ज्ञान बढ़ता है।
- नए-नए शब्दों, मुहावरों तथा वाक्य रचना का ज्ञान होता है।
- शब्द-भंडार में वृद्धि होती है, इससे भाषिक योग्यता बढ़ती है।
- प्रसंगानुसार शब्दों के अनेक अर्थ तथा अलग-अलग प्रयोग से परिचित होते हैं।
- गद्यांश के मूलभाव को समझकर अपने शब्दों में व्यक्त करने की दक्षता बढ़ती है। इससे हमारे अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि होती है।
- भाषिक योग्यता में वृद्धि होती है।
अपठित गद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करें –
अपठित गद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करेंअपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए
- गद्यांश को एक बार सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए।
- पहली बार में समझ में न आए अंशों, शब्दों, वाक्यों को गहनतापूर्वक पढ़ना चाहिए।
- गद्यांश का मूलभाव अवश्य समझना चाहिए।
- यदि कुछ शब्दों के अर्थ अब भी समझ में नहीं आते हों तो उनका अर्थ गद्यांश के प्रसंग में जानने का प्रयास करना चाहिए।
- अनुमानित अर्थ को गद्यांश के अर्थ से मिलाने का प्रयास करना चाहिए।
- गद्यांश में आए व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। अब प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर गद्यांश में
- खोजने का प्रयास करना चाहिए।
- शीर्षक समूचे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता हुआ कम से कम एवं सटीक शब्दों में होना चाहिए।
- प्रतीकात्मक शब्दों एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए।
- मूल भाव या संदेश संबंधी प्रश्नों का जवाब पूरे गद्यांश पर आधारित होना चाहिए।
- प्रश्नों का उत्तर देते समय यथासंभव अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए।
- उत्तर की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होनी चाहिए।
- प्रश्नों का जवाब गद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए, आपके अपने विचार या राय से नहीं।
- अति लघूत्तरात्मक तथा लघूत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा अलग-अलग होती है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए।
- प्रश्नों का जवाब सटीक शब्दों में देना चाहिए, घुमा-फिराकर जवाब देने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए –
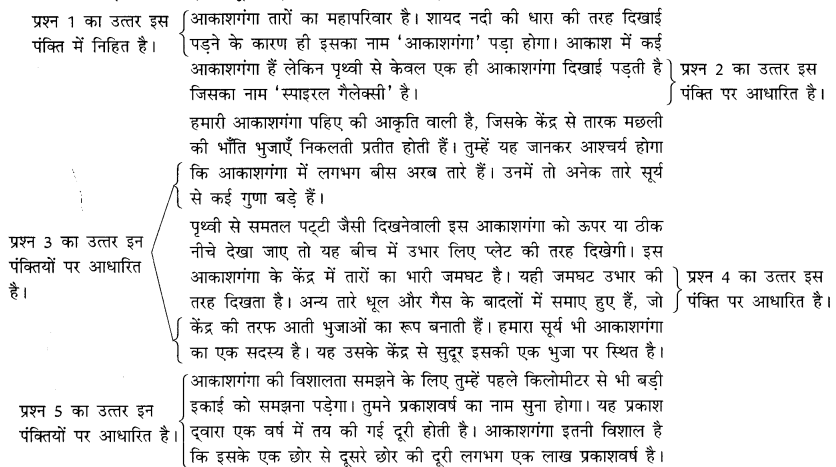
प्रश्नः 1.
उदाहरण (उत्तर सहित)
1. भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन इस बात की आशंका किसी को नहीं थी कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल न सिर्फ खेतों में, बल्कि खेतों से बाहर मंडियों तक में होने लगेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग खाद्यान्न की गुणवत्ता के लिए सही नहीं है, लेकिन जिस रफ़्तार से देश की आबादी बढ़ रही है, उसके मद्देनज़र फ़सलों की अधिक पैदावार ज़रूरी थी। समस्या सिर्फ रासायनिक खादों के प्रयोग की ही नहीं है। देश के ज़्यादातर किसान परंपरागत कृषि से दूर होते जा रहे हैं।
दो दशक पहले तक हर किसान के यहाँ गाय, बैल और भैंस खूटों से बँधे मिलते थे। अब इन मवेशियों की जगह ट्रैक्टर-ट्राली ने ले ली है। परिणामस्वरूप गोबर और घूरे की राख से बनी कंपोस्ट खाद खेतों में गिरनी बंद हो गई। पहले चैत-बैसाख में गेहूँ की फ़सल कटने के बाद किसान अपने खेतों में गोबर, राख और पत्तों से बनी जैविक खाद डालते थे। इससे न सिर्फ खेतों की उर्वरा-शक्ति बरकरार रहती थी, बल्कि इससे किसानों को आर्थिक लाभ के अलावा बेहतर गुणवत्ता वाली फसल मिलती थी।
2. ताजमहल, महात्मा गांधी और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र-इन तीन बातों से दुनिया में हमारे देश की ऊँची पहचान है। ताजमहल भारत की अंतरात्मा की, उसकी बहुलता की एक धवल धरोहर है। यह सांकेतिक ताज आज खतरे में है। उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है।
मजहबी दर्द को गांधी दूर करता गया। दुनिया जानती है, गांधीवादी नहीं जानते हैं। गांधीवादी उस गांधी को चाहते हैं जो कि सुविधाजनक है। राजनीतिज्ञ उस गांधी को चाहते हैं जो कि और भी अधिक सुविधाजनक है। आज इस असुविधाजनक गांधी का पुनः आविष्कार करना चाहिए, जो कि कड़वे सच बताए, खुद को भी औरों को भी।
अंत में तीसरी बात लोकतंत्र की। हमारी जो पीड़ा है, वह शोषण से पैदा हुई है, लेकिन आज विडंबना यह है कि उस शोषण से उत्पन्न पीड़ा का भी शोषण हो रहा है। यह है हमारा ज़माना, लेकिन अगर हम अपने पर विश्वास रखें और अपने पर स्वराज लाएँ तो हमारा ज़माना बदलेगा। खुद पर स्वराज तो हम अपने अनेक प्रयोगों से पा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी भूलें स्वीकार करना, खुद को सुधारना बहुत आवश्यक होगा
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययनों और संयुक्त राष्ट्र की मानव-विकास रिपोर्टों ने भारत के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता के साथ-साथ बाल मृत्यु-दर और मातृ मृत्यु दर का ग्राफ़ काफ़ी ऊँचा रहने के तथ्य भी बार-बार जाहिर किए हैं। यूनिसेफ़ की रिपोर्ट बताती है कि लड़कियों की दशा और भी खराब है।
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाद, बालिग होने से पहले लड़कियों को ब्याह देने के मामले दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा भारत में होते हैं। मातृ-मृत्यु दर और शिशु मृत्यु-दर का एक प्रमुख कारण यह भी है। यह रिपोर्ट ऐसे समय जारी हुई है जब बच्चों के अधिकारों से संबंधित वैश्विक घोषणा-पत्र के पच्चीस साल पूरे हो रहे हैं। इस घोषणा-पत्र पर भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देशों ने भी हस्ताक्षर किए थे। इसका यह असर ज़रूर हुआ कि बच्चों की सेहत, शिक्षा, सुरक्षा से संबंधित नए कानून बने, मंत्रालय या विभाग गठित हुए, संस्थाएँ और आयोग बने।
घोषणा-पत्र से पहले की तुलना में कुछ सुधार भी दर्ज हआ है। पर इसके बावजूद बहुत सारी बातें विचलित करने वाली हैं। मसलन, देश में हर साल लाखों बच्चे गुम हो जाते हैं। लाखों बच्चे अब भी स्कूलों से बाहर हैं। श्रम-शोषण के लिए विवश बच्चों की तादाद इससे भी अधिक है वे स्कूल में पिटाई और घरेलू हिंसा के शिकार होते रहते हैं।
परिवार के स्तर पर देखें तो संतान का मोह काफ़ी प्रबल दिखाई देगा, मगर दूसरी ओर बच्चों के प्रति सामाजिक संवेदनशीलता बहुत क्षीण है। कमज़ोर तबकों के बच्चों के प्रति तो बाकी समाज का रवैया अमूमन असहिष्णुता का ही रहता है। क्या ये स्वस्थ समाज के लक्षण हैं?
4. चंपारण सत्याग्रह के बीच जो लोग गांधी जी के संपर्क में आए वे आगे चलकर देश के निर्माताओं में गिने गए। चंपारण में गांधी जी न सिर्फ सत्य और अहिंसा का सार्वजनिक हितों में प्रयोग कर रहे थे बल्कि हलुवा बनाने से लेकर सिल पर मसाला पीसने और चक्की चलाकर गेहूँ का आटा बनाने की कला भी उन बड़े वकीलों को सिखा रहे थे, जिन्हें गरीबों की अगुवाई की जिम्मेदारी सौंपी जानी थी। अपने इन आध्यात्मिक प्रयोगों के माध्यम से वे देश की गरीब जनता की सेवा करने और उनकी तकदीर बदलने के साथ देश को आजाद कराने के लिए समर्पित व्यक्तियों की एक ऐसी जमात तैयार करना चाह रहे थे जो सत्याग्रह की भट्ठी में उसी तरह तपकर निखरे, जिस तरह भट्ठी में सोना तपकर निखरता और कीमती बनता है।
गांधी जी की मान्यता थी कि एक प्रतिष्ठित वकील और हज़ामत बनाने वाले हज़्ज़ाम में पेशे के लिहाज़ से कोई फ़र्क नहीं, दोनों की हैसियत एक ही हैं। उन्होंने पसीने की कमाई को सबसे अच्छी कमाई माना और शारीरिक श्रम को अहमियत देते हुए उसे उचित प्रतिष्ठा व सम्मान दिया था। कोई काम बड़ा नहीं, कोई काम छोटा नहीं, इस मान्यता को उन्होंने प्राथमिकता दी ताकि साधन शुद्धता की बुनियाद पर एक ठीक समाज खड़ा हो सके। आज़ाद हिंदुस्तान आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और आत्म-सम्मानित देश के रूप में विश्व-बिरादरी के बीच अपनी एक खास पहचान बनाए और फिर उसे बरकरार भी रखे।
5. आज की नारी संचार प्रौद्योगिकी, सेना, वायुसेना, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विज्ञान वगैरह के क्षेत्र में न जाने किन-किन भूमिकाओं में कामयाबी के शिखर छू रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जहाँ आज की महिलाओं ने अपनी छाप न छोड़ी हो। कह सकते हैं कि आधी नहीं, पूरी दुनिया उनकी है। सारा आकाश हमारा है। पर क्या सही मायनों में इस आज़ादी की आँच हमारे सुदूर गाँवों, कस्बों या दूरदराज के छोटे-छोटे कस्बों में भी उतनी ही धमक से पहुँच पा रही है? क्या एक आज़ाद, स्वायत्त मनुष्य की तरह अपना फैसला खुद लेकर मज़बूती से आगे बढ़ने की हिम्मत है उसमें?
बेशक समाज बदल रहा है मगर यथार्थ की परतें कितनी बहुआयामी और जटिल हैं जिन्हें भेदकर अंदरूनी सच्चाई तक पहुँच पाना आसान नहीं। आज के इस रंगीन समय में नई बढ़ती चुनौतियों से टकराती स्त्री की क्रांतिकारी आवाजें हम सबको सुनाई दे रही हैं, मगर यही कमाऊ स्त्री जब समान अधिकार और परिवार में लोकतंत्र की अनिवार्यता पर बहस करती या सही मायनों में लोकतंत्र लाना चाहती है तो वहाँ इसकी राह में तमाम धर्म, भारतीय संस्कृति, समर्पण, सहनशीलता, नैतिकता जैसे सामंती मूल्यों की पगबाधाएँ खड़ी की जाती हैं। नारी की सच्ची स्वाधीनता का अहसास तभी हो पाएगा जब वह आज़ाद मनुष्य की तरह भीतरी आज़ादी को महसूस करने की स्थितियों में होगी।

6. अकाल के बीच भी अच्छे काम और अच्छे विचार का एक सुंदर छोटा सा उदाहरण राजस्थान के अलवर क्षेत्र का है जहाँ तरुण भारत संघ पिछले बीस बरस से काम कर रहा है। वहाँ पहले अच्छा विचार आया तालाबों का, हर नदी, नाले को छोटे-छोटे बाँधों से बाँधने का। इस तरह वहाँ आसपास के कुछ और जिलों के कोई 600 गाँवों ने बरसों तक वर्षा की एकएक बूंद को सहेज लेने का काम चुपचाप किया। इन तालाबों, बाँधों ने वहाँ सूखी पड़ी पाँच नदियों को ‘सदानीरा’ का नाम वापस दिलाया।
अच्छे विचारों से अच्छा काम हुआ और फिर आई चुनौती भरे अकाल की पहली सूचना। नदियों में, तालाबों में, कुओं में वहाँ तब भी पानी लबालब भरा था। फिर भी इस क्षेत्र के लोगों ने, किसानों ने आज से सात-आठ माह पहले यह निर्णय किया कि पानी कम गिरा है इसलिए ऐसी फ़सलें नहीं बोनी चाहिए जिनकी प्यास ज़्यादा होती है। तो कम पानी लेने वाली फ़सलें लगाई गईं। इसमें उन्हें कुछ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा पर आज यह क्षेत्र अकाल के बीच में एक बड़े हरे द्वीप की तरह खड़ा है। यहाँ सरकार को न तो टैंकरों से पानी ढोना पड़ रहा है न अकाल राहत का पैसा बाँटना पड़ा है। गाँव के लोग, किसी के आगे हाथ नहीं पसार रहे हैं।
उनका माथा ऊँचा है। पानी के उम्दा काम ने उनके स्वाभिमान की भी रक्षा की है। अलवर में नदियाँ एक दूसरे से जोड़ी नहीं गई हैं। यहाँ के लोग अपनी नदियों से, अपने तालाबों से जुड़े हैं। यहाँ पैसा नहीं बहाया गया है, पसीना बहाया है, लोगों ने और उनके अच्छे काम और अच्छे विचारों ने अकाल को एक दर्शक की तरह पाल के किनारे खड़ा कर दिया है।
विदेशी शासन के अन्याय-अनीति के विरोध में उन्होंने जितना बड़ा सामूहिक प्रतिरोध संगठित किया, उसकी मिसाल संसार के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलती। पर इसमें उन्होंने सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखा कि इस प्रतिरोध में कहीं भी कटुता, प्रतिशोध की भावना अथवा कोई भी ऐसी अनैतिक बात न हो जिसके लिए विश्व मंच पर भारत का माथा नीचा हो ऐसा गांधी जी ने इसलिए किया क्योंकि वे मानते थे कि बंधुत्व, मैत्री, सद्भावना, स्नेह-सौहार्द आदि गुण मानवता-रूपी टहनी के ऐसे पुष्प हैं जो सर्वदा सुगंधित रहते हैं।
8. तिलक ने हमें स्वराज का सपना दिया और गांधी ने उस सपने को दलितों और स्त्रियों से जोड़कर एक ठोस सामाजिक अवधारणा के रूप में देश के सामने ला रखा। स्वतंत्रता के उपरांत बड़े-बड़े कारखाने खोले गए, वैज्ञानिक विकास भी हुआ, बड़ी-बड़ी योजनाएँ भी बनीं, किंतु गांधीवादी मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सीमित होती चली गई। दुर्भाग्य से गांधी के बाद गांधीवाद को कोई ऐसा व्याख्याकार न मिला जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भो में गांधी के सोच की समसामयिक व्याख्या करता। सो यह विचार लोगों में घर करता चला गया कि गांधीवादी विकास का मॉडल धीमे चलने वाला और तकनीकी प्रगति से विमुख है। उस पर ध्यान देने से हम आधुनिक वैज्ञानिक युग की दौड़ में पिछड़ जाएँगे। कहना न होगा कि कुछ लोगों की पाखंडी जीवन शैली ने भी इस धारणा को और पुष्ट किया।
इसका परिणाम यह हुआ कि देश में बुनियादी तकनीकी और औद्योगिक प्रगति तो आई पर देश के सामाजिक और वैचारिकढाँचे में ज़रूरी बदलाव नहीं लाए गए। सो तकनीकी विकास ने समाज में व्याप्त व्यापक फटेहाली, धार्मिक कूपमंडूकता और जातिवाद को नहीं मिटाया।

9. कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र यदि कहीं कमज़ोर है तो उसकी एक बड़ी वजह हमारे राजनीतिक दल हैं। वे प्रायः अव्यवस्थित हैं, अमर्यादित हैं और अधिकांशतः निष्ठा और कर्मठता से संपन्न नहीं हैं। हमारी राजनीति का स्तर प्रत्येक दृष्टि से गिरता जा रहा है। लगता है उसमें सुयोग्य और सच्चरित्र लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र के मूल में लोकनिष्ठा होनी चाहिए, लोकमंगल की भावना और लोकानुभूति होनी चाहिए और लोकसंपर्क होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में इन आधारभूत तत्वों की कमी होने लगी है, इसलिए लोकतंत्र कमज़ोर दिखाई पड़ता है।
हम प्रायः सोचते हैं कि हमारा देश-प्रेम कहाँ चला गया, देश के लिए कुछ करने, मर-मिटने की भावना कहाँ चली गई ? त्याग और बलिदान के आदर्श कैसे, कहाँ लुप्त हो गए? आज हमारे लोकतंत्र को स्वार्थांधता का घुन लग गया है। क्या राजनीतिज्ञ, क्या अफसर, अधिकांश यही सोचते हैं कि वे किस तरह से स्थिति का लाभ उठाएँ, किस तरह एक-दूसरे का इस्तेमाल करें। आम आदमी अपने आपको लाचार पाता है और ऐसी स्थिति में उसकी लोकतांत्रिक आस्थाएँ डगमगाने लगती हैं।
लोकतंत्र की सफलता के लिए हमें समर्थ और सक्षम नेतृत्व चाहिए, एक नई दृष्टि, एक नई प्रेरणा, एक नई संवेदना, एक नया आत्मविश्वास, एक नया संकल्प और समर्पण आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए हम सब अपने आप से पूछे कि हम देश के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या कर सकते हैं? और हम सिर्फ पूछकर ही न रह जाएँ, बल्कि संगठित होकर समझदारी, विवेक और संतुलन से लोकतंत्र को सफल और सार्थक बनाने में लग जाएँ।
10. एक ज़माना था जब मुहल्लेदारी पारिवारिक आत्मीयता से भरी होती थी। सब मिल-जुलकर रहते थे। हारी-बीमारी, खुशी-गम सब में लोग एक दूसरे के साथ थे। किसी का किसी से कुछ छिपा नहीं था। आज के लोगों को शायद लगे कि लोगों की अपनी ‘प्राइवेसी’ क्या रही होगी, लेकिन इस ‘प्राइवेसी’ के नाम पर ही तो हम एक-दूसरे से कटते रहे और कटते-कटते ऐसे अलग हुए कि अकेले पड़ गए। पहले अलग चूल्हे-चौके हुए, फिर अलग मकान लेकर लोग रहने लगे, निजी स्वतंत्रता को अपनी नई परिभाषा देकर यह एकाकीपन हमने स्वयं अपनाया है। मुहल्ले में आपस में चाहे जितनी चखचख हो, यह थोड़े ही संभव था कि बाहर का कोई आकर किसी को कड़वी बात कह जाए। पूरा मोहल्ला टिड्डी-दल की तरह उमड़ पड़ता था।
देखते-देखते ज़माना हवा हो गया। मुहल्लेदारी टूटने लगी, आबादी बढ़ी, महँगाई बढ़ी, पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ दुर्लभ हो गई वह थी आपसी लगाव, अपनापन। लोगों की आँखों का शील मर गया।
देखते-देखते कैसा रंग बदला है। लोग अपने-आप में सिमटकर पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। सारे नाते-रिश्तों को उन्होंने ताक पर रख दिया है, तब फिर पड़ोसी से उन्हें क्या लेना-देना है। यह नीरस महानगरीय सभ्यता महानगरों से चलकर कस्बों और देहातों तक को अपनी चपेट में ले चुकी है। मकानों में रहने वाले एक-दूसरे को नहीं जानते। इन जगहों में आदमी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। यदि आपको फ़्लैट नंबर मालूम नहीं है तो उसी बिल्डिंग में जाकर भी वांछित व्यक्ति को नहीं ढूँढ़ पाएँगे। ऐसी जगहों में किसी प्रकार के संबंधों की अपेक्षा ही कहाँ की जा सकती है?
NCERT Solutions for Class 10 Hindi – A
NCERT Solutions for Class 10 Hindi Kshitij
NCERT Solutions for Class 10 Hindi Kshitij Bhag 2 क्षितिज भाग 2
काव्य – खंड
- Chapter 1 पद
- Chapter 2 राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद
- Chapter 3 सवैया और कवित्त
- Chapter 4 आत्मकथ्य
- Chapter 5 उत्साह और अट नहीं रही
- Chapter 6 यह दंतुरहित मुस्कान और फसल
- Chapter 7 छाया मत छूना
- Chapter 8 कन्यादान
- Chapter 9 संगतकार
गद्य – खंड
- Chapter 10 नेताजी का चश्मा
- Chapter 11 बालगोबिन भगत
- Chapter 12 लखनवी अंदाज़
- Chapter 13 मानवीय करुणा की दिव्या चमक
- Chapter 14 एक कहानी यह भी
- Chapter 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन
- Chapter 16 नौबतखाने में इबादत
- Chapter 17 संस्कृति
NCERT Solutions for Class 10 Hindi Kritika
NCERT Solutions for Class 10 Hindi Kritika Bhag 2 कृतिका भाग 2
- Chapter 1 माता का आँचल
- Chapter 2 जॉर्ज पंचम की नाक
- Chapter 3 साना-साना हाथ जोड़ि
- Chapter 4 एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा!
- Chapter 5 मैं क्यों लिखता हूँ?
NCERT Solutions for Class 10 Hindi – B
NCERT Solutions for Class 10 Hindi Sparsh
NCERT Solutions for Class 10 Hindi Sparsh Bhag 2 स्पर्श भाग 2
काव्य – खंड
- Chapter 1 साखी
- Chapter 2 पद
- Chapter 3 दोहे
- Chapter 4 मनुष्यता
- Chapter 5 पर्वत प्रदेश में पावस
- Chapter 6 मधुर-मधुर मेरे दीपक जल
- Chapter 7 तोप
- Chapter 8 कर चले हम फ़िदा
गद्य – खंड
- Chapter 9 आत्मत्राण
- Chapter 10 बड़े भाई साहब
- Chapter 11 डायरी का एक पन्ना
- Chapter 12 तताँरा-वामीरो कथा
- Chapter 13 तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र
- Chapter 14 गिरगिट
- Chapter 15 अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले
- Chapter 16 पतझर में टूटी पत्तियाँ
- Chapter 17 कारतूस
NCERT Solutions for Class 10 Hindi Sanchayan
NCERT Solutions for Class 10 Hindi Sanchayan Bhag संचयन भाग 2

Post a Comment
इस पेज / वेबसाइट की त्रुटियों / गलतियों को यहाँ दर्ज कीजिये
(Errors/mistakes on this page/website enter here)